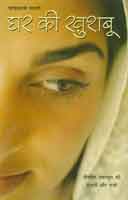|
गजलें और शायरी >> दूसरा बनबास दूसरा बनबाससुरेश कुमार
|
546 पाठक हैं |
|||||||
कैफ़ी साहब की मशहूर-ओ-मारूफ़ ग़ज़लों और नज़्मों का मजमुआ
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
प्राक्कथन
कैफ़ी आज़मी उर्दू शायरी की तरक़्क़ी-पसन्द तहरीक के प्रतिनिधि शायर हैं।
फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, असरारुल हक़ मज़ाज़, जाँनिसार अख़्तर, मुइन अहसन
जज़्वी, अली सरदार ज़ाफ़री,. मज़रूह सुल्तानपुरी और कैफ़ी आज़मी प्रगतिशील
उर्दू कविता के ऐसे स्वर्णिम हस्ताक्षर हैं जिनके बिना आधुनिक उर्दू कविता
की प्रगतिशील धारा का इतिहास लिखा जाना सम्भव ही नहीं है। इन सभी शायरों
ने मनुष्य की बेहतरी के लिए एक शोषणमुक्त समाज की कल्पना की और अपनी शायरी
के माध्यम से समाज को प्रेम और सद्भाव का संदेश देते हुए समाज को मानवता
के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहे।
समकालीन उर्दू शायरी श्रृंखला के अन्तर्गत कैफ़ी आज़मी को शामिल करने पर कुछ मित्रों द्वारा यह प्रश्न उठाया जाना स्वाभाविक है कि उर्दू शायरी की प्रगतिशील धारा के उन्नायकों के रूप में प्रतिष्ठित और कुछ अर्थों में ‘क्लासिक’ हो चुके कैफ़ी आज़मी को इस श्रृंखला में शामिल करने का आधार क्या है ? जब इस श्रृंखला को प्रकाशित करने की योजना बन रही थी तब मेरे मस्तिष्क में प्रायः यह स्पष्ट था कि कोई भी वरिष्ठ शायर चाहे वह किसी भी तहरीक से जुड़ा रहा हो, सन् 1960 के बाद भी यदि रचनाकर्म में सक्रिय रहा है तो उसे इस श्रृंखला में शामिल किया जायेगा। हम सभी जानते हैं कि अपनी लम्बी अस्वस्थता के बावजूद कैफ़ी आज़मी अन्तिम समय तक अपने रचनाकर्म से कभी विरत नहीं हुए। इन अर्थों में वे अपने बाद की पीढ़ी के शायरों निदा फ़ाज़ली और जावेद अख़्तर के भी समकालीन ठहरते हैं।
1992 में कुछ संकीर्णतावादियों ने जिस तरह का वातावरण हमारे देश में उत्पन्न कर दिया था और जब धर्मनिरपेक्षता का दावा करने वाले अच्छे-अच्छों के पाँव डगमगाने लगे थे, तब अपनी अशक्तता और अस्वस्थता की स्थिति में भी कैफ़ी आज़मी न सिर्फ़ एक पहाड़ की तरह उस साम्प्रदायिक आँधी के ख़िलाफ़ खड़े रहे बल्कि ‘दूसरा बनबास’ जैसी मार्मिक और ऐतिहासिक महत्व की नज़्म भी उन्होंने लिखी। हिन्दी और उर्दू काव्य में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण मुश्किल से ही मिलेगा। कला, साहित्य और विचारधारा के प्रति ऐसी प्रतिबद्धता प्रायः दुर्लभ होती है और आज के समय में तो शायद असम्भव भी। वे सिर्फ़ सिद्धांततः ही नहीं बल्कि व्यावहारिक रूप में भी सच्चे मार्क्सवादी थे।
‘दूसरा बनबास’ कैफ़ी आज़मी की प्रतिनिधि ग़ज़लों और नज़्मों का ऐसा संकलन है जो उनकी काव्य-यात्रा के हर पल का न सिर्फ़ साक्ष्य देता है बल्कि उनके मानव-प्रेम, जीवन-संघर्ष और मनुष्य की अनन्तता के प्रति उनकी अटूट आस्था की कहानी भी स्वयं बयान करता है। इस संग्रह की रूपरेखा को अन्तिम रूप देने तक श्रीमती शबाना आज़मी और श्री जावेद अख़्तर ने क़दम-क़दम पर जिस आत्मीयता के साथ मुझे अपना सहयोग दिया है, उसे शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए सम्भव नहीं है।
बहरहाल, ‘दूसरा बनबास’ आपके हाथों में है और मुझे पूरा यकीन है कि इसकी रचनाओं के माध्यम से न सिर्फ़ कैफ़ी आज़मी के महान व्यक्तित्व अपितु हमारे दौर की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों को समझने में भी पाठकों को आसानी होगी।
107, ज्वालापुरी, जी.टी. रोड
अलीगढ़—202001
समकालीन उर्दू शायरी श्रृंखला के अन्तर्गत कैफ़ी आज़मी को शामिल करने पर कुछ मित्रों द्वारा यह प्रश्न उठाया जाना स्वाभाविक है कि उर्दू शायरी की प्रगतिशील धारा के उन्नायकों के रूप में प्रतिष्ठित और कुछ अर्थों में ‘क्लासिक’ हो चुके कैफ़ी आज़मी को इस श्रृंखला में शामिल करने का आधार क्या है ? जब इस श्रृंखला को प्रकाशित करने की योजना बन रही थी तब मेरे मस्तिष्क में प्रायः यह स्पष्ट था कि कोई भी वरिष्ठ शायर चाहे वह किसी भी तहरीक से जुड़ा रहा हो, सन् 1960 के बाद भी यदि रचनाकर्म में सक्रिय रहा है तो उसे इस श्रृंखला में शामिल किया जायेगा। हम सभी जानते हैं कि अपनी लम्बी अस्वस्थता के बावजूद कैफ़ी आज़मी अन्तिम समय तक अपने रचनाकर्म से कभी विरत नहीं हुए। इन अर्थों में वे अपने बाद की पीढ़ी के शायरों निदा फ़ाज़ली और जावेद अख़्तर के भी समकालीन ठहरते हैं।
1992 में कुछ संकीर्णतावादियों ने जिस तरह का वातावरण हमारे देश में उत्पन्न कर दिया था और जब धर्मनिरपेक्षता का दावा करने वाले अच्छे-अच्छों के पाँव डगमगाने लगे थे, तब अपनी अशक्तता और अस्वस्थता की स्थिति में भी कैफ़ी आज़मी न सिर्फ़ एक पहाड़ की तरह उस साम्प्रदायिक आँधी के ख़िलाफ़ खड़े रहे बल्कि ‘दूसरा बनबास’ जैसी मार्मिक और ऐतिहासिक महत्व की नज़्म भी उन्होंने लिखी। हिन्दी और उर्दू काव्य में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण मुश्किल से ही मिलेगा। कला, साहित्य और विचारधारा के प्रति ऐसी प्रतिबद्धता प्रायः दुर्लभ होती है और आज के समय में तो शायद असम्भव भी। वे सिर्फ़ सिद्धांततः ही नहीं बल्कि व्यावहारिक रूप में भी सच्चे मार्क्सवादी थे।
‘दूसरा बनबास’ कैफ़ी आज़मी की प्रतिनिधि ग़ज़लों और नज़्मों का ऐसा संकलन है जो उनकी काव्य-यात्रा के हर पल का न सिर्फ़ साक्ष्य देता है बल्कि उनके मानव-प्रेम, जीवन-संघर्ष और मनुष्य की अनन्तता के प्रति उनकी अटूट आस्था की कहानी भी स्वयं बयान करता है। इस संग्रह की रूपरेखा को अन्तिम रूप देने तक श्रीमती शबाना आज़मी और श्री जावेद अख़्तर ने क़दम-क़दम पर जिस आत्मीयता के साथ मुझे अपना सहयोग दिया है, उसे शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए सम्भव नहीं है।
बहरहाल, ‘दूसरा बनबास’ आपके हाथों में है और मुझे पूरा यकीन है कि इसकी रचनाओं के माध्यम से न सिर्फ़ कैफ़ी आज़मी के महान व्यक्तित्व अपितु हमारे दौर की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों को समझने में भी पाठकों को आसानी होगी।
107, ज्वालापुरी, जी.टी. रोड
अलीगढ़—202001
-सुरेश कुमार
(1)
मैं ढूँढ़ता हूँ जिसे वो जहाँ नहीं मिलता
नयी ज़मीन नया आसमाँ नहीं मिलता
नयी ज़मीन नया आसमाँ भी मिल जाये
नये बशर1 का कहीं कुछ निशाँ नहीं मिलता
वो तेग़2 मिल गयी जिससे हुआ है क़त्ल मिरा
किसी के हाथ का उस पर निशाँ नहीं मिलता
वो मेरा गाँव है, वो मेरे गाँव के चूल्हे
कि जिनमें शोले तो शोले, धुआँ नहीं मिलता
जो इक खुदा नहीं मिलता तो इतना मातम क्यों
यहाँ तो कोई मेरा हमज़बाँ नहीं मिलता
खड़ा हूँ कब से मैं चेहरों के एक जंगल में
तुम्हारे चेहरे का कुछ भी यहाँ नहीं मिलता
नयी ज़मीन नया आसमाँ नहीं मिलता
नयी ज़मीन नया आसमाँ भी मिल जाये
नये बशर1 का कहीं कुछ निशाँ नहीं मिलता
वो तेग़2 मिल गयी जिससे हुआ है क़त्ल मिरा
किसी के हाथ का उस पर निशाँ नहीं मिलता
वो मेरा गाँव है, वो मेरे गाँव के चूल्हे
कि जिनमें शोले तो शोले, धुआँ नहीं मिलता
जो इक खुदा नहीं मिलता तो इतना मातम क्यों
यहाँ तो कोई मेरा हमज़बाँ नहीं मिलता
खड़ा हूँ कब से मैं चेहरों के एक जंगल में
तुम्हारे चेहरे का कुछ भी यहाँ नहीं मिलता
1. मनुष्य 2. तलवार
(2)
हाथ आकर लगा गया कोई
मेरा छप्पर उठा गया कोई
लग गया इक मशीन में मैं भी
शहर में ले के आ गया कोई
मैं खड़ा था कि पीठ पर मेरी
इश्तिहार1 इक लगा गया कोई
ये सदी धूप को तरसती है
जैसे सूरज को खा गया कोई
ऐसी मँहगाई है कि चेहरा भी
बेच के अपना खा गया कोई
अब वो अरमान हैं न वो सपने
सब कबूतर उड़ा गया कोई
वो गये जब से ऐसा लगता है
छोटा-मोटा खुदा गया कोई
मेरा बचपन भी साथ ले आया
गाँव से जब भी आ गया कोई
मेरा छप्पर उठा गया कोई
लग गया इक मशीन में मैं भी
शहर में ले के आ गया कोई
मैं खड़ा था कि पीठ पर मेरी
इश्तिहार1 इक लगा गया कोई
ये सदी धूप को तरसती है
जैसे सूरज को खा गया कोई
ऐसी मँहगाई है कि चेहरा भी
बेच के अपना खा गया कोई
अब वो अरमान हैं न वो सपने
सब कबूतर उड़ा गया कोई
वो गये जब से ऐसा लगता है
छोटा-मोटा खुदा गया कोई
मेरा बचपन भी साथ ले आया
गाँव से जब भी आ गया कोई
1. विज्ञापन
(3)
पत्थर के खुदा वहाँ भी पाये
हम चाँद से आज लौट आये
दीवारें तो हर तरफ़ खड़ी हैं
क्या हो गये मेहरबान साये
जंगल की हवाएँ आ रही हैं
काग़ज़ का ये शहर उड़ न जाये
लैला ने नया जनम लिया है
है क़ैस कोई जो दिल लगाये
है आज ज़मीं का गुस्ल-ए-सेहत1
जिस दिल में हो जितना खून लाये
सहरा-सहरा लहू के ख़ेमे
फिर प्यासे लब-ए-फ़रात2 आये
हम चाँद से आज लौट आये
दीवारें तो हर तरफ़ खड़ी हैं
क्या हो गये मेहरबान साये
जंगल की हवाएँ आ रही हैं
काग़ज़ का ये शहर उड़ न जाये
लैला ने नया जनम लिया है
है क़ैस कोई जो दिल लगाये
है आज ज़मीं का गुस्ल-ए-सेहत1
जिस दिल में हो जितना खून लाये
सहरा-सहरा लहू के ख़ेमे
फिर प्यासे लब-ए-फ़रात2 आये
1. स्वास्थ्य-स्नान 2. मीठे और ठण्डे पानी
के किनारे (फरात : इराक की एक)
(4)
क्या जाने किसी की प्यास बुझाने किधर गयीं
उस सर पे झूम के जो घटाएँ गुज़र गयीं
दीवाना पूछता है ये लहरों से बार-बार
कुछ बस्तियाँ यहाँ थीं बताओ किधर गयीं
अब जिस तरफ़ से चाहो गुज़र जाये कारवाँ
वीरानियाँ तो सब मिरे दिल में उतर गयीं
पैमाना1 टूटने का कोई ग़म नहीं मुझे
ग़म है तो ये कि चाँदनी रातें बिखर गयीं
पाया भी उनको खो भी दिया चुप भी हो रहे
इक मुख़्तसर-सी2 रात में सदियाँ गुज़र गयीं
उस सर पे झूम के जो घटाएँ गुज़र गयीं
दीवाना पूछता है ये लहरों से बार-बार
कुछ बस्तियाँ यहाँ थीं बताओ किधर गयीं
अब जिस तरफ़ से चाहो गुज़र जाये कारवाँ
वीरानियाँ तो सब मिरे दिल में उतर गयीं
पैमाना1 टूटने का कोई ग़म नहीं मुझे
ग़म है तो ये कि चाँदनी रातें बिखर गयीं
पाया भी उनको खो भी दिया चुप भी हो रहे
इक मुख़्तसर-सी2 रात में सदियाँ गुज़र गयीं
1. मदिरा पात्र 2. छोटी-सी
(5)
जो वो मिरे न रहे मैं भी कब किसी का रहा
बिछड़ के उनसे सलीक़ा न ज़िन्दगी का रहा
लबों से उड़ गया जुगनू की तरह नाम उसका
सहारा अब मिरे घर में न रोशनी का रहा
गुज़रने को तो हज़ारों ही क़ाफ़िले गुज़रे
ज़मीं पे नक्श-ए-क़दम1 बस किसी-किसी का रहा
बिछड़ के उनसे सलीक़ा न ज़िन्दगी का रहा
लबों से उड़ गया जुगनू की तरह नाम उसका
सहारा अब मिरे घर में न रोशनी का रहा
गुज़रने को तो हज़ारों ही क़ाफ़िले गुज़रे
ज़मीं पे नक्श-ए-क़दम1 बस किसी-किसी का रहा
1. पद-चिह्न
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i